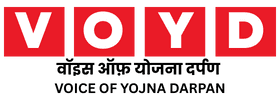इमेज स्रोत, Getty Imagesइमेज कैप्शन, (प्रतीकात्मक तस्वीर)….मेंAuthor, शेरिलान मोलान पदनाम, बीबीसी न्यूज़, मुंबई1 अगस्त 2025जुलाई के आख़िर में वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने भारत में सहमति से सेक्स की क़ानूनी उम्र (जो इस समय 18 साल है) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तर्क रखे. इस बहस के साथ किशोरों के बीच यौन संबंध को अपराध मानने के मुद्दे पर चर्चा फिर तेज हो गई.जयसिंह का कहना है कि 16 से 18 साल के किशोरों के बीच सहमति से बने यौन संबंध न शोषण हैं और न अत्याचार. उनका कहना है कि ऐसे मामलों को आपराधिक मुक़दमों के दायरे से बाहर रखा जाए.अपने लिखित तर्क में उन्होंने कहा, “उम्र पर आधारित कानूनों का उद्देश्य बच्चों को शोषण से बचाना होना चाहिए, न कि सहमति पर आधारित और उम्र के लिहाज से उचित संबंधों को अपराध मान लेना.”लेकिन केंद्र सरकार इस मांग का विरोध कर रही है. उसका कहना है कि अगर ऐसे अपवाद को मंज़ूरी दी जाए तो 18 साल से कम उम्र के बच्चे, जिन्हें भारतीय क़ानून में नाबालिग माना जाता है, उनके शोषण और अत्याचार का ख़तरा और बढ़ जाएगा.यह मामला सहमति की परिभाषा पर नई बहस छेड़ रहा है. सवाल उठ रहा है कि क्या भारतीय क़ानूनों, ख़ासकर 2012 के पॉक्सो क़ानून में बदलाव करके 16 से 18 साल वाले किशोरों के बीच सहमति से बने संबंधों को इस क़ानून के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए.इमेज स्रोत, Getty Imagesविशेषज्ञों की राय क्या है?बाल अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर किशोरों को इस दायरे से बाहर किया जाए तो उनकी स्वतंत्रता बनी रहती है. वहीं विरोध करने वालों का मानना है कि ऐसा करने से मानव तस्करी और बाल विवाह जैसे अपराध बढ़ सकते हैं.विशेषज्ञ यह सवाल भी उठाते हैं कि अगर किसी किशोर के साथ अत्याचार हो जाए तो क्या वह सबूत देने का बोझ उठा पाएगा. सबसे अहम सवाल यह बनता है कि सहमति की उम्र तय करने का अधिकार किसके पास होना चाहिए और इन क़ानूनों का वास्तविक लाभ किसे मिलता है.दुनिया के कई देशों की तरह भारत को भी ‘सहमति से सेक्स’ की सही उम्र तय करने में कठिनाई रही है. अमेरिका में यह उम्र अलग-अलग राज्यों में अलग होती है, जबकि भारत में यह पूरे देश के लिए समान रखी गई है.भारत में सहमति से यौन संबंध बनाने की क़ानूनी उम्र यूरोप के ज़्यादातर देशों और ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों की तुलना में काफी ज़्यादा है. इन देशों में ये उम्र 16 साल है.1860 में जब भारत का आपराधिक क़ानून लागू हुआ तब यह उम्र 10 साल थी. 1940 में संशोधन कर इसे 16 साल किया गया.पॉक्सो क़ानून ने अगला बड़ा बदलाव किया और 2012 में सहमति की उम्र 18 साल कर दी गई. इसके बाद 2013 में आपराधिक क़ानूनों में बदलाव कर इसे शामिल किया गया और 2024 में लागू हुए नए आपराधिक क़ानून में भी यही उम्र जारी रखी गई.उनका तर्क है कि मौजूदा क़ानून सहमति पर आधारित किशोर संबंधों को अपराध मान लेता है. कई बार वयस्क इस क़ानून का इस्तेमाल ऐसे रिश्तों को रोकने या दबाने के लिए करते हैं, ख़ासकर लड़कियों के मामले में.देश में यौन संबंध का विषय अब भी खुलकर बात करने योग्य नहीं माना जाता, जबकि कई अध्ययनों में सामने आया है कि लाखों भारतीय किशोर यौन रूप से सक्रिय हैं.फ़ॉउंडेशन फ़ॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन-मुस्कान की सह-संस्थापक शर्मिला राजे कहती हैं, “हम ऐसे समाज में रहते हैं जो जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर बंटा हुआ है. यही कारण है कि सहमति की उम्र से जुड़े क़ानून के ग़लत इस्तेमाल का ख़तरा और बढ़ जाता है.”इमेज स्रोत, Getty Imagesइमेज कैप्शन, भारत के कई स्कूलों में पाठ्यक्रम के हिस्से के तौर पर सेक्स एजुकेशन नहीं है2022 में कर्नाटक हाईकोर्ट का निर्देशसाल 2022 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने, क़ानूनी सुधारों पर सुझाव देने वाले भारत के विधि आयोग को यह निर्देश दिया था कि पॉक्सो क़ानून के तहत सहमति की उम्र पर दोबारा विचार किया जाए ”ताकि ज़मीनी हकीकत को ध्यान में रखा जा सके.”अदालत ने ऐसे कई मामलों का ज़िक्र किया था, जहां 16 साल से अधिक उम्र की लड़कियां प्रेम संबंध में पड़ीं और यौन संबंध बनाए, लेकिन बाद में लड़के पर पॉक्सो और आपराधिक क़ानून के तहत बलात्कार और अपहरण के आरोप लगा दिए गए.अगले साल विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उम्र घटाने से इनकार कर दिया, लेकिन यह सिफ़ारिश की कि 16 से 18 साल के बच्चों के सहमति वाले रिश्तों में सज़ा तय करते समय अदालतें ‘न्यायिक विवेक’ का इस्तेमाल करें.हालांकि इस सिफ़ारिश को अभी तक क़ानूनी रूप नहीं दिया गया है, लेकिन देशभर की अदालतें इस सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए अपील सुनने, ज़मानत देने, बरी करने या कुछ मामलों को ख़ारिज करने जैसे फ़ैसले दे रही हैं. इसमें वे मामले के तथ्य और पीड़ित की गवाही को ध्यान में रखती हैं.शर्मिला राजे समेत कई बाल अधिकार कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि इस प्रावधान को क़ानून में शामिल किया जाए ताकि इसके इस्तेमाल में एकरूपता रहे. अगर इसे सिर्फ सुझाव के तौर पर छोड़ दिया गया तो अदालतें इसे नजरअंदाज कर सकती हैं.अप्रैल में मद्रास हाईकोर्ट ने एक मामले में बरी करने के फ़ैसले को पलट दिया. इस मामले में 17 साल की लड़की 23 साल के अभियुक्त के साथ रिश्ते में थी और जब उसके माता-पिता ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी तो वह अभियुक्त के साथ अपने घर से चली गई. अदालत ने अभियुक्त को 10 साल की कैद की सजा सुनाई.एनफोल्ड प्रैक्टिव हेल्थ ट्रस्ट (एक बाल अधिकार संस्था) की शोधकर्ता श्रुति रामकृष्णन ने इस फ़ैसले पर इंडियन एक्सप्रेस अख़बार में लिखा है, “अदालत ने पॉक्सो क़ानून को ज्यों का त्यों शब्दों के आधार पर लागू किया,” और इस फ़ैसले को उन्होंने “न्याय की गंभीर विफलता” कहा.इमेज स्रोत, Getty Imagesइमेज कैप्शन, (प्रतीकात्मक तस्वीर)”कई लोगों के लिए पूरी प्रक्रिया ही सज़ा”जयसिंह का तर्क है कि सिर्फ़ सज़ा सुनाते समय न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अभियुक्त को तब भी लंबी जांच और मुक़दमे की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है.भारत की न्यायिक व्यवस्था अपने धीमे कामकाज के लिए जानी जाती है, जहां हर स्तर पर लाखों मामले लंबित हैं. इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फ़ंड की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक़ जनवरी 2023 तक सिर्फ़ पॉक्सो मामलों की सुनवाई के लिए बनी विशेष अदालतों में करीब ढाई लाख मामले लंबित थे.जयसिंह कहती हैं, “कई लोगों के लिए पूरी प्रक्रिया ही सजा बन जाती है.”वह आगे कहती हैं, “हर मामले को अलग-अलग देखकर जजों पर छोड़ देना भी सही समाधान नहीं है, क्योंकि इससे फ़ैसलों में असमानता आ सकती है और पक्षपात की संभावना को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है.”वकील और बाल अधिकार कार्यकर्ता भुवन ऋभु का कहना है कि अगर बिना शर्त ऐसे अपवादों को मंज़ूरी दे दी जाए तो इसका ग़लत इस्तेमाल अपहरण, मानव तस्करी और बाल विवाह जैसे मामलों में हो सकता है. वह न्यायिक विवेक के साथ-साथ न्याय व्यवस्था में सुधार की वकालत करते हैं.वह कहते हैं, “हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें केस तय समय में निपटें. इसके साथ ही पीड़ितों के लिए बेहतर पुनर्वास सुविधाएं और मुआवजे की व्यवस्था भी होनी चाहिए.”हालांकि ‘हक: सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स’ की सह-संस्थापक एनाक्षी गांगुली, इंदिरा जयसिंह के पक्ष में हैं.वह कहती हैं, “सिर्फ़ इसलिए बदलाव से नहीं बच सकते क्योंकि हमें डर है कि क़ानून का ग़लत इस्तेमाल होगा.”वह कहती हैं कि जयसिंह की यह दलील नई नहीं है, पिछले कई सालों में कई कार्यकर्ता और विशेषज्ञ ऐसे सुझाव पहले भी दे चुके हैं.गांगुली का कहना है, “अगर क़ानून को प्रभावी और प्रासंगिक बनाए रखना है तो उन्हें समाज में हो रहे बदलावों के साथ तालमेल बैठाना होगा.”बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.
Source link
RELATED ARTICLES