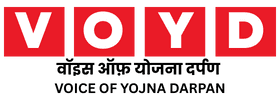इमेज कैप्शन, ख़्वाजा क़ुतुबुद्दीन बख़्तियार काकी का मज़ार….मेंAuthor, मिर्ज़ा एबी बेगपदनाम, बीबीसी उर्दू, नई दिल्ली30 अगस्त 2025यह आज से लगभग 225 साल पहले की बात है, जब मुग़ल राजधानी केवल एक हफ़्ते के लिए दिल्ली के लाल क़िले से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण के इलाक़े महरौली ले जाई गई थी.महरौली को राजधानी बनाने के जश्न के तौर पर वहां आम के बाग़ों में झूले डाले गए, मुर्ग़ों की लड़ाई हुई, बैलों की भिड़ंत पर शर्तें लगीं, पतंगबाज़ी हुई, कुश्ती और तैराकी के मुक़ाबले हुए और उत्सव व मनोरंजन के इसी माहौल में एक सूफ़ी बुज़ुर्ग के मज़ार पर फूलों की चादर भी चढ़ाई गई.महरौली में होने वाला यह जश्न दरअसल अकबर शाह द्वितीय (1808-1837) के बेटे मिर्ज़ा जहांगीर की रिहाई के मौक़े पर आयोजित किया गया था.अकबर शाह द्वितीय की पत्नी मुमताज़ महल बड़े बेटे सिराजुद्दीन ज़फ़र (जो बाद में बहादुर शाह ज़फ़र के नाम से गद्दी पर बैठे और आख़िरी मुग़ल बादशाह हुए) की बजाय अपने मंझले बेटे मिर्ज़ा जहांगीर को तख़्त पर बैठाना चाहती थीं.बीबीसी हिंदी के व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करेंमुमताज़ महल की इस ख़्वाहिश की वजह से अकबर शाह द्वितीय ने मंझले बेटे मिर्ज़ा जहांगीर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, मगर यह फ़ैसला अंग्रेज़ रेज़िडेंट को मंज़ूर नहीं था.महरौली का जश्न और मिर्ज़ा जहांगीरभारत में उस वक़्त कहने को तो मुग़ल बादशाहों की ही सरकार थी, लेकिन असल में हुक्म कंपनी का ही चलता था.मिर्ज़ा जहांगीर को उत्तराधिकारी घोषित करने के मामले पर अकबर शाह द्वितीय और अंग्रेज़ रेज़िडेंट के बीच कहा-सुनी हो गई. इसी दौरान शहज़ादे मिर्ज़ा जहांगीर ने अंग्रेज़ रेज़िडेंट पर तमंचा (पिस्तौल) तान कर गोली चला दी.हालांकि अंग्रेज़ रेज़िडेंट अर्चिबाल्ड सेटन उस गोली से बच गए, लेकिन इस जुर्म में जहांगीर को क़ैद कर लिया गया और दिल्ली से इलाहाबाद भेज दिया गया.मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग अपनी किताब ‘फूल वालों की सैर’ में लिखते हैं कि मां मुमताज़ ने शहज़ादे जहांगीर की रिहाई के लिए महरौली स्थित ख़्वाजा क़ुतुबुद्दीन बख़्तियार काकी के मज़ार पर मन्नत मांगी थी कि अगर उनके बेटे की रिहाई हो जाती है तो वह उनकी क़ब्र पर फूलों की एक मसहरी चढ़ाएंगी.आख़िरकार शहज़ादे जहांगीर की रिहाई हुई और महरौली में एक हफ़्ते तक चलने वाला यह जश्न बख़्तियार काकी की दरगाह पर मांगी गई उसी मन्नत के पूरे होने पर आयोजित किया गया.सात दिनों तक जश्न का माहौल रहा और आम लोग इससे इतने ख़ुश हुए कि यह एक परंपरा बन गई और इसे हर साल मनाया जाने लगा. यहां तक कि बहादुर शाह ज़फ़र ने सन 1857 के विद्रोह के दौरान भी इस जश्न को मनाया, हालांकि यह मुग़ल दौर का आख़िरी जश्न साबित हुआ.सूफ़ी परंपरा और बख़्तियार काकीइमेज स्रोत, Preeti mann/BBCइस्लामी दुनिया, ख़ासकर भारत में सूफ़ीवाद के विशेषज्ञ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफ़ेसर सैयद ज़हीर हुसैन जाफ़री ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि मिर्ज़ा जहांगीर की रिहाई पर महरौली में मनाया जाने वाला यह जश्न बख़्तियार काकी की मौत के लगभग 600 साल बाद की घटना है. इससे उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा होता है और उनके मज़ार पर यह परंपरा आज भी जारी है.इस जश्न को ‘सैर-ए-गुलफ़रोशां’ यानी ‘फूल वालों की सैर’ का नाम दिया गया. हालांकि 1942 में सरकारी संरक्षण में इसका आयोजन बंद हो गया, लेकिन यह परंपरा लगातार आज भी जारी है.प्रोफ़ेसर सैयद ज़हीर हुसैन जाफ़री ने बताया कि इस जश्न के दौरान बख़्तियार काकी की दरगाह के रास्ते में स्थित ‘योगमाया’ मंदिर पर फूलों का पंखा भी चढ़ाया गया, जो इसे भारत की हिंदू-मुस्लिम साझा संस्कृति का प्रतीक बनाता है.प्रोफ़ेसर जाफ़री ने कहा कि आम लोगों की श्रद्धा और उनकी यादों ने उन्हें सरकार की पाबंदियों के बावजूद उन दरगाहों से जोड़े रखा है.जामिया मिलिया इस्लामिया में इस्लामिक स्टडीज़ विभाग के पूर्व प्रमुख प्रोफ़ेसर अख़्तरुल वासे ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि भारत में तीन तरीक़ों से इस्लाम आया.पहला, व्यापार के ज़रिए, जिसकी शुरुआत दक्षिण भारत से हुई.दूसरा, सैनिक अभियानों के ज़रिए, जो महमूद ग़ज़नवी और मोहम्मद ग़ौरी जैसे आक्रमणकारियों की शक्ल में सामने आया.तीसरा, सूफ़ियों और वली अल्लाह (सूफ़ी संतों) के ज़रिए.और इसी तीसरे तरीक़े की एक कड़ी बख़्तियार काकी हैं, जिन्होंने दिल्ली के आसपास स्थित एक गांव को अपना ठिकाना बनाया, जो अब महरौली कहलाता है.इमेज स्रोत, Preeti mann/BBCऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी में इतिहास के शिक्षक और ऑक्सफ़ोर्ड सेंटर फ़ॉर इस्लामिक स्टडीज़ के फ़ेलो मोईन अहमद निज़ामी ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि यह वह दौर था जब भारत में उलेमा और सूफ़ी आए, जो महत्वपूर्ण शहरों के बजाय गांव-देहातों में जाकर ठहरते थे. “यहीं से वह आम लोगों से संपर्क में आए. इस्लाम के प्रचार-प्रसार में उनकी भूमिका अहम है.”हालांकि इन सूफ़ियों ने बादशाहों से दूरी बनाए रखी, लेकिन बख़्तियार काकी दिल्ली के दूसरे बादशाह सुल्तान इल्तुतमिश (अल्तमश) को बहुत महत्व देते थे. सुल्तान ने ही उन्हें शैख़ुल इस्लाम की उपाधि दी थी, हालांकि बख़्तियार काकी ने इस उपाधि को ठुकरा दिया.लेकिन उनके बाद के ज़माने में उन्हें ‘क़ुतुब अल-अक़ताब’ यानी ‘क़ुतुबों का क़ुतुब’ (संतों का संत) क़रार दिया गया. मोईन अहमद निज़ामी के अनुसार उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त था कि उन्होंने अपने दौर के तीन बड़े सूफ़ियों, शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी और शहाबुद्दीन सुहरवर्दी से आशीर्वाद और ज्ञान लिया. साथ ही समरक़ंद में मोईनुद्दीन संजरी (चिश्ती) से भी मिले और उनके समूह में शामिल हुए.मोईन अहमद निज़ामी के मुताबिक़, बख़्तियार काकी को मोईनुद्दीन सजरी (चिश्ती) की ओर से ख़िर्क़ा-ए-ख़िलाफ़त सौंपा गया. (ख़िर्क़ा एक मामूली कपड़ा होता है, जिसे देकर कोई सूफ़ी अपने उत्तराधिकारी को मान्यता देता है.) इसके बाद उन्हें दिल्ली की ओर कूच करने को कहा गया.बख़्तियार काकी मध्य-पूर्व में फ़रग़ना घाटी के ओश (जो अब किर्गिस्तान में है) से चलकर भारत पहुंचे थे. अबुल फ़ज़ल की रचना ‘आईन-ए-अकबरी’ के अनुसार उनके पिता का नाम सैयद कमालुद्दीन मूसा अल-हुसैनी था.उनका असल नाम बख़्तियार था, लेकिन उनकी शिक्षा-दीक्षा और श्रेष्ठता की वजह से उन्हें क़ुतुबुद्दीन की उपाधि दी गई. उनकी वंशावली मूसा अल-काज़िम, जाफ़र अल-सादिक़ और मोहम्मद अल-बाक़र से होती हुई इमाम ज़ैनुल आबेदीन बिन हुसैन और फिर हज़रत अली तक पहुंचती है.कहा जाता है कि जब सूफ़ी दरवेश मोईनुद्दीन चिश्ती ‘ओश’ से गुज़रे तो उन्होंने बख़्तियार काकी को दिल्ली जाने का आदेश दिया और बताया कि उनकी शिक्षा-दीक्षा की रोशनी वहीं फैलनी है.ध्यान रहे कि बख़्तियार काकी हज़रत मोईनुद्दीन चिश्ती के पहले ख़लीफ़ा थे.क़ुतुबुद्दीन बख़्तियार को ‘काकी’ क्यों कहा जाता है?इमेज स्रोत, Getty Imagesइतिहासकारों के अनुसार यह उपाधि उन्हें उनके ‘चमत्कार और करामात’ की वजह से दी गई. सूफ़ियों की ज़िंदगी बेहद सरल होती थी और ग़रीबी-तंगहाली उनकी परंपरा का हिस्सा मानी जाती थी. यही हाल क़ुतुबुद्दीन बख़्तियार का भी था.ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि जब उनके घर में भूखों रहने की नौबत आती, तो उनकी बीवी उनके इशारे पर पड़ोस के नान बाई (रोटी बनाने वाले) से क़र्ज़ ले लिया करती थीं. लेकिन एक दिन बख़्तियार काकी ने अपनी बीवी को क़र्ज़ लेने से मना कर दिया.इस पर उनकी बीवी ने पूछा, “तो फिर हम खाएंगे कहां से?” बख़्तियार काकी ने जवाब दिया कि जब ज़रूरत हो, घर के फ़लां कोने से जाकर ‘काक’ ले लिया करना. काक एक तरह की रोटी को कहा जाता था. इसके बाद से उनकी बीवी जब भी खाने की ज़रूरत महसूस करतीं, घर के उसी ख़ास कोने में जातीं, जहां रोटी पहले से मौजूद होती.पड़ोस में रहने वाले नान बाई ने देखा कि बहुत दिनों से ख़्वाजा के घर से न तो क़र्ज़ लिया गया और न ही रोटी. उसे लगा कि कहीं ख़्वाजा उससे नाराज़ तो नहीं हो गए. यह जानने के लिए उसने अपनी बीवी को ख़्वाजा बख़्तियार के घर हाल पूछने भेजा.जब नानबाई की बीवी ने ख़्वाजा बख़्तियार की बीवी से रोटी या क़र्ज़ न लेने की वजह पूछी तो ख़्वाजा की बीवी ने उन्हें यह राज़ बता दिया. कहा जाता है कि उस दिन के बाद घर के कोने से ‘काक’ मिलनी बंद हो गई, लेकिन उनकी इस ‘करामात’ की चर्चा हर तरफ़ फैल गई और उन्हें ‘काकी’ कहा जाने लगा.प्रोफ़ेसर जाफ़री कहते हैं कि सूफ़ियों और वलियों से करिश्मों का जुड़ना लोकप्रिय कहानियों का हिस्सा है, लेकिन गंभीर इतिहासकारों की किताबों में इसका उल्लेख नहीं मिलता.उन्होंने मध्यकाल के मशहूर इतिहासकार ज़िया उद्दीन बर्नी का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली के शेख़ हज़रत निज़ामुद्दीन के बारे में विस्तार से लिखा है. बर्नी बताते हैं कि हर धर्म और समुदाय के लोग उनके पास खिंचे चले आते थे, लेकिन किसी करिश्मे का ज़िक्र नहीं किया.मोईन अहमद निज़ामी के अनुसार, “भारत में ये दरगाहें इसलिए फली-फूलीं क्योंकि वहां लोगों के दुख-दर्द दूर किए जाते थे, उन्हें खाना मिलता था और हर तरह के लोगों के ठहरने की व्यवस्था होती थी. भारत में यह परंपरा इन्हीं सूफ़ी संतों के ज़रिए परवान चढ़ी और उनके सेवा-भाव से लोगों में उनके लिए श्रद्धा पैदा हुई.अगर बख़्तियार काकी को उनकी ज़िंदगी में सुल्तान इल्तुतमिश से सम्मान मिला, तो लोदी और मुग़ल सुल्तानों ने भी उन्हें श्रद्धा की नज़र से देखा.कहा जाता है कि सुल्तान इल्तुतमिश एक जंग से लौटने के बाद आराम करने के बजाय अपने पीर-ओ-मुर्शिद क़ुतुबुद्दीन बख़्तियार काकी के दीदार को चले गए ताकि उनसे अपनी श्रद्धा जता सकें. उन्होंने दिल्ली में उनके ही सम्मान में क़ुतुब मीनार बनवाया. हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह सुल्तान क़ुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर है, जिन्होंने इसके निर्माण की शुरुआत की थी.जेएनयू से पीएचडी करने वाले मोहम्मद हयात, जो महरौली में रहते हैं, बताते हैं कि आख़िरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने वहीं अपनी क़ब्र के लिए जगह तय की थी. आज भी वहां ‘ज़फ़र महल’ मौजूद है. उन्होंने बीबीसी को एक तस्वीर दिखाते हुए कहा कि यही वह जगह है, जहां बहादुर शाह ज़फ़र दफ़न होना चाहते थे.गांधी, नेहरू और फूल वालों की सैरइमेज स्रोत, National Gandhi Museum’द हिंदू’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, 1947 में भारत विभाजन के दौरान दंगाइयों ने बख़्तियार काकी के मज़ार की बेअदबी की, उसकी जालियां तोड़ी गईं और महरौली में बड़े पैमाने पर क़त्ल-ए-आम हुआ. उस समय महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल करते हुए मांग की थी कि दरगाह को उर्स के लिए समय पर ठीक हालत में लाया जाए और 72 घंटों के भीतर मज़ार की मरम्मत कराई जाए.मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किताब ‘इंडिया विंस फ़्रीडम’ में इसका ज़िक्र किया है. उन्होंने लिखा कि 1948 में जब गांधीजी ने दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों और हिंसा को हमेशा के लिए ख़त्म करने की मांग के साथ अपनी अंतिम भूख हड़ताल शुरू की, तो सभी समुदायों के नेताओं ने उन पर अनशन तोड़ने का दबाव डाला. गांधीजी ने अनशन ख़त्म करने के लिए छह शर्तें रखीं, जिनमें से एक यह थी कि हिंदू और सिख प्रायश्चित स्वरूप ख़्वाजा बख़्तियार काकी के मज़ार की मरम्मत करवाएं, जिसे दंगों में नुक़सान पहुंचा था.जब महात्मा गांधी ने ख़्वाजा बख़्तियार काकी के सालाना उर्स के मौक़े पर उनके मजार की ज़ियारत की, तो उनके साथ एक बड़ी भीड़ थी. इसके बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ‘फूल वालों की सैर’ की परंपरा को फिर से शुरू किया. मोहम्मद हयात बताते हैं कि अब यह सात के बजाय तीन दिन का जश्न है, जिसमें ख़्वाजा बख़्तियार काकी के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई जाती है और पास स्थित मंदिर में पंखा चढ़ाया जाता है.कहा जाता है कि ख़्वाजा बख़्तियार काकी भारत में क़व्वाली की कला लाने वाले पहले शेख़ थे. उन्होंने यहां समा (सूफ़ी नृत्य) की परंपरा शुरू की, जो बाद में चिश्ती सिलसिले में आम हो गई.मोईनुद्दीन निज़ामी बताते हैं कि ख़्वाजा बख़्तियार काकी की पैदाइश और परवरिश ओश में हुई थी, जो हल्लाजी सूफ़ी सिलसिले का केंद्र था. ख़्वाजा काकी समा की महफ़िलों के बहुत शौक़ीन थे. वह इस परंपरा को भारत लेकर आए और ख़ुद भी बड़ी रुचि से इनमें शामिल होते थे.वह ख़ुद एक शायर थे और उनकी रचनाओं का संग्रह भी उपलब्ध है. एक दिन उनके पास अहमद जामी नाम के शायर ने एक शेर पढ़ा, जिसके बाद उन पर ऐसा हाल तारी हुआ यानी ऐसी मदहोशी में चले गए कि वह चार दिन तक समा की हालत में रहे और उसी हालत में उनकी मौत हो गई.वह यह शेर पढ़ते और झूमते रहते: कुश्तगान-ए-ख़ंजर-ए-तस्लीम रा/ हर ज़मां अज़ ग़ैब जान-ए-दीगर अस्त. (वह लोग जो अल्लाह की राह में ख़ुशी से क़ुर्बान होते हैं, वह हर ज़माने में दूसरी दुनिया से नई ज़िंदगी पाते हैं).उनका मज़ार महरौली में ज़फ़र महल से सटा क़ुतुब मीनार के पास है. महरौली को कुछ लोग ‘मेहर-ए-वली’ भी कहते हैं, यानी वह इलाक़ा जहां संतों की बरकत और मेहरबानियां बरसती हों.उर्स के अलावा यहां एक बड़ा समारोह ‘सैर-ए-गुलफ़रोशां’ (फूल वालों की सैर) भी होता है. इस उत्सव को जवाहरलाल नेहरू के प्रोत्साहन पर 1962 में फिर से शुरू किया गया. तब से यह सिलसिला लगातार जारी है. अब कई राज्यों की ओर से इस मौक़े पर मज़ार पर फूलों की चादर और मंदिर पर पंखा चढ़ाया जाता है. यह स्थल सभी धर्मों के लिए आस्था का केंद्र है, जहां कई अन्य सूफ़ी संतों और शेख़ों की क़ब्रें भी हैं.बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित
Source link
RELATED ARTICLES